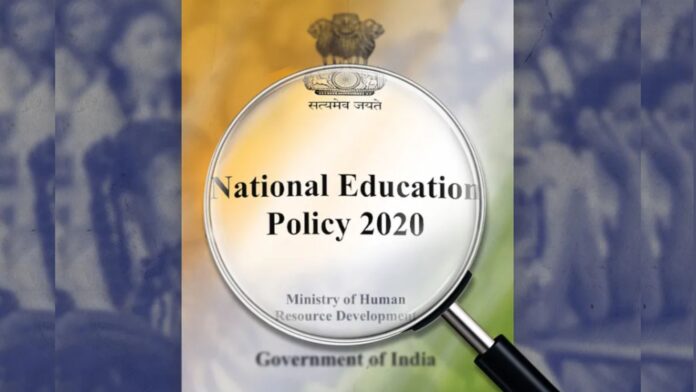शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल
ऋषभ कुमार मिश्र
इस महीने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को चार वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर राज्य मात्रात्मक आंकड़ों, जिनमें संसाधन और सुविधा विस्तार का उल्लेख होगा, के सहारे अपनी प्रगति गाथा गाएगा। औपचारिक शिक्षा तंत्र की संस्थाएं अपने-अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार उपलब्धियों का बखान करेंगी। कुछ नई आकर्षक शब्दावलियों के सहारे नए अभियानों, योजनाओं और कार्यक्रमों का आरंभ होगा। इन प्रयासों के द्वारा आमजन के सामने एक सकारात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन इस चित्र को यदि कोई ‘ज़ूम’ करके देखने की कोशिश करेगा तो बहुत कुछ बिखरा-बिखरा दिखने लगेगा।
उदाहरण के लिए बारहवीं पास बच्चे स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति में है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक विद्यालय में उपस्थिति के तरीक़ों एवं तंत्र को लेकर आक्रोश में हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कोर्ट-कचहरी का मामला लगातार ख़बरों में बना हुआ है। विश्वविद्यालयों में नौकरी के लिए शिक्षित युवा जोड़-तोड़ कर रहे हैं। सरकार के सख़्त आदेश के पालन में विद्यालयों के लिए आनन-फानन में बनाई गई योजनाएं धरातल पर हांफ़ रही हैं। कुल मिलाकर औपचारिक शिक्षा के इस रूपहले पर्दे को देखते हुए बार-बार ‘गुणवत्ता’, ‘विकास’ और ‘समावेशन’ जैसे शिक्षा के लिए रूढ़ हो गए शब्दों के सहारे ‘भारत’ और ‘विकास’ के रिश्ते को समझाया जाएगा लेकिन धरातल पर यथास्थिति क़ायम है। इस यथास्थिति के कारणों की पड़ताल करें तो समझ में आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की संस्तुतियां प्रासंगिक हैं लेकिन इन्हें कार्यरूप देने के दौरान हमारी व्यवस्था की जड़ता अवरोधक का कार्य कर रही है। इस तरह की कुछ जड़ताओं को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।
प्रथम, विशेषज्ञों द्वारा निर्मित योजनाओं का नौकरशाही द्वारा क्रियान्वयन शिक्षा से संबंधित नवाचारों को गौण कर रहा है। केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं बन रही हैं, उनमें स्थानीयता, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता, नवाचार के अवसर आदि को रखा जा रहा है। इन योजनाओं को बनाते समय विशेषज्ञों सहित ज़मीनी कार्यकर्ताओं की सलाह भी ली जा रही है। लेकिन जैसे ही कोई योजना सलाहकार या विशेषज्ञ समिति की संस्तुति से निकलकर फ़ाइलों पर पहुंचती है, वैसे ही इससे जुड़े शिक्षा के आयाम गौण हो जाते हैं। इसके बदले योजना का भविष्य नौकरशाही के रवैये से तय होने लगता है। अब शिक्षा के सुनहरे शब्द जैसे – बदलाव, सशक्तिकरण, नवाचार की आज़ादी आदि के बदले वित्त का वितरण, योजना को क्रियान्वित करने वालों की निगरानी और प्रशासनिक पचड़े प्रमुख हो जाते हैं। अब योजना बदलाव के विचारों और अभिप्रेरणाओं से नहीं चलती बल्कि सरकारी आदेशों से चलने लगती है। इस तरह के आदेश जब तक केंद्रीय स्तर से निचले स्तर तक पहुचंते हैं, तब तक सुधार के बदले ‘व्यवहार में बदलाव’ इसका लक्ष्य हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण शिक्षकों की उपस्थिति के लिए ऑनलाइन माध्यमों का प्रयोग है। शैक्षिक सुधार की किसी भी योजना में इस तरह की संस्तुति कदापि नहीं होती कि जिस शिक्षक को आप प्रयोग और नवाचार की ज़िम्मेदारी देने जा रहे हैं, उनकी नीयत पर शक करें। फिर भी, विद्यालयों में प्रयोग और नवाचार के लिए शिक्षकों की उपस्थिति को एक संकेतक मानते हुए उनकी उपस्थिति पर ‘सख़्त निगरानी’ का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग से शिक्षक उपस्थित तो हो जाएंगें लेकिन उनकी अभिप्रेरणा और स्वतंत्र प्रयोग करने की चेष्टा प्रतिरोध में बदल जाएगी और उनका प्रतिरोधात्मक व्यवहार शैक्षिक सुधारों को जड़ कर देगा।
द्वितीय, यह पूरी नीति ‘चाहिए के मकड़ जाल’ में फंसी है। पिछले चार वर्षों में इस नीति के क्रियान्वयन से संबंधित अनगिनत आयोजन हुए। इन आयोजनों में भारतीय ज्ञान परंपरा, आनुभविक अधिगम, कौशल विकास, समग्र शिक्षा और भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस तरह के आयोजनों का एक मोटा ख़ाका खींचा जाए तो पता चलता है कि इनमें प्रारंभिक या परिचय स्तर पर नीति का उल्लेख होता है। इसके बाद व्याख्याता निजी मंतव्य और अनुभवों के आधार पर नीति की सराहना या कुछ नई कठिन अवधारणाओं पर चर्चा कर दूर की कौड़ी लाने का प्रयास करते हैं। विषय विशेषज्ञ नीति में कही गई प्रमुख बातों को बार-बार अलग-अलग ढंग से अलग-अलग उदाहरणों के साथ व्याख्यायित करते हैं। इस तरह से ये आयोजन नीति की मुख्य संस्तुतियों को नक्कारख़ाने की तूती की तरह बजाए जाने की रस्मअदायगी बन गए हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के बाद से ‘भारतीय ज्ञान परंपरा’ एक आकर्षक शब्द के रूप में हमारे सामने आया है। इससे जुड़ी हज़ारों संगोष्ठियां और कार्यशालाएं हो रही हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर कार्यशाला-संगोष्ठी में भारतीय ज्ञान परंपरा के अर्थ और उसकी व्यापकता को बताया जा रहा है। इसके बावजू़द कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है कि इस पूरे उद्यम से उनका कक्षा शिक्षण कैसे बदलेगा? उन्हें अपने अभ्यास के लिए क्या नए सूत्र मिल रहे हैं? उन्हें अर्थ और प्रासंगिकता बताकर प्रयोग के लिए समर्थ मान लेना नीति की संस्तुति को कमज़ोर कर रहा है।
तृतीय, वर्तमान परिवेश में हम शैक्षिक संस्थानों का अवलोकन करें तो पाएंगें कि ज़्यादातर शैक्षिक कर्मी ज्ञानवान और बदलाव के लिए अभिप्रेरित कर्ता बनने के स्थान पर सत्तानिष्ठ बने रहना पसंद कर रहे हैं। इस कारण नीति के क्रियान्वयन के लिए जिस ज्ञानाधार, कुशलता और प्रदर्शन में बदलाव की अपेक्षा है उसके बदले केवल सत्ता को ख़ुश करने के उपाय हो रहे हैं। यह सत्ता केवल दल विशेष या विचारधारा विशेष से संबंधित नहीं है। अगर विद्यालय में प्रधानाध्यापक की सत्ता है, खंड शिक्षा अधिकारी की सत्ता है तो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विभागाध्यक्ष और संकायप्रमुखों से लेकर कुलपति तक की सत्ता है। इस सबके बीच शिक्षक संघों और कर्मचारी संघों को जोड़ दें तो शैक्षिक परिसरों में व्याप्त ‘राग दरबारी’ को समझा जा सकता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि पढ़ना-पढ़ना एक रूटीन गतिविधि मात्र है और सत्ता संबंध साधना सोद्देश्य और नियोजित गतिविधि है। शैक्षिक कर्मियों की मननशीलता का उपयोग शैक्षिक सुधारों के लिए हो या न हो लेकिन सत्ता की शान में ज़रूर हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक छद्म श्रेष्ठता बोध से युक्त ऐसे समूह बन गए हैं जो शैक्षिक मुद्दों और नीति के क्रियान्वयन के बारे में उपदेश दे रहे हैं। वे मान रहे हैं कि उन्हें सुनने वाले उनका पालन करेंगे लेकिन सुनने वालों का अपना ‘मोटिव’ है। ऐसे श्रोता अगले स्तर पर ख़ुद को उपदेशक मान लेते हैं और वे नए श्रोताओं को उपदेश दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में परिणाम यह है कि उपदेशों के बीच वास्तव में बदलाव के लिए किया जाने वाला कार्य गौण हो गया है। कुछ करने के बदले, ‘क्या करना चाहिए’ को बताने की परिपाटी यथास्थिति को बनाए हुए है।
चतुर्थ, अकादमिक संस्थानों की प्रकृति प्रशासनिक संस्थानों जैसी होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य ने शैक्षिक सुधारों की गति को तेज़ करने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसका एक परिणाम यह हुआ है कि अकादमिक संस्थानों को सेना और पुलिस के प्रशासनिक ढांचे की तरह बनाया जा रहा है। ‘युद्धस्तर पर कार्यवाही‘ जैसे मुहावरे चला दिए गए हैं। एक केंद्रीय संस्थान में दोपहर के भोजनावकाश के बाद घंटी बजाकर कर्मियों को बुलाने का भी प्रयोग किया गया। कुछ संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाओं को लेने के बाद उनकी रिपोर्ट प्रशासन को भेजने को कहा गया। इससे हमारे परिसरों में अकादमिक सौहार्द्र और विश्वास के बजाय संदेह और अविश्वास का रिश्ता पनप रहा है, जो जवाबदेही के नाम पर प्रदत्त कार्य की खानापूर्ति की संस्कृति को जन्म दे रहा है। अकादमिक संस्थानों की प्रशासनिक प्रकृति में बदलाव का एक अन्य परिणाम अवलोकनीय है। जैसे-जैसे अकादमिक संस्थानों की प्रकृति प्रशासनिक संस्थानों की तरह होती जाती है, वैसे-वैसे इसके भागीदार अपनी भूमिका बदलने लगते हैं। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा में विभागों और संकायों की संरचना कुछ इस तरह की बन गई है कि वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे वरिष्ठ शिक्षक शैक्षिक प्रशासनिक पदों जैसे- सचिव, कुलपति और निदेशक आदि बनकर पुनर्यौवन प्राप्त करना चाहते हैं। नवनियुक्त शिक्षक बेहतर अवसरों की तलाश में ख़ेमेबाज़ी द्वारा सत्ता के चक्रव्यूह को भेदना चाह रहे हैं। इस सबके बीच कक्षा में पढ़ाने और शोध की यथास्थिति क़ायम है। नीति और उसकी संस्तुतियां कक्षा में शब्दजाल बुनने का माध्यम बन कर रह गई हैं। ऐसा मान लिया गया है कि पढ़ने-लिखने के बजाय प्रशासन से निकटता अधिक लाभदायक है। इस लाभ की ‘ठकुरसुहाती‘ हर रोज़ गाई जा रही है।
अब तक इस लेख में आपके सामने जो शब्द चित्र खींचा गया, उसमें निराशाजनक निहितार्थ खोजने से पहले हमें स्वयं से यह सवाल पूछना होगा कि क्या ये प्रवृत्तियां हमारे समय के औपचारिक शिक्षा तंत्र की सच्चाई नहीं है? क्या इन्हीं परिस्थितियों और दबावों के कारण औपचारिक शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता ख़तरे में है? क्या शिक्षा से जुड़े कर्मी ख़ुद को इन प्रवृत्तियों के बीच उलझा हुआ नहीं पा रहे हैं? इन सवालों पर विचार करते हुए नीति और नीयत का फ़र्क़ सामने आता है। इन सवालों के उत्तर उन जड़ताओं से परिचय कराते हैं जो शिक्षा की यथास्थिति को क़ायम रखे हुए हैं।
साभार